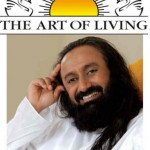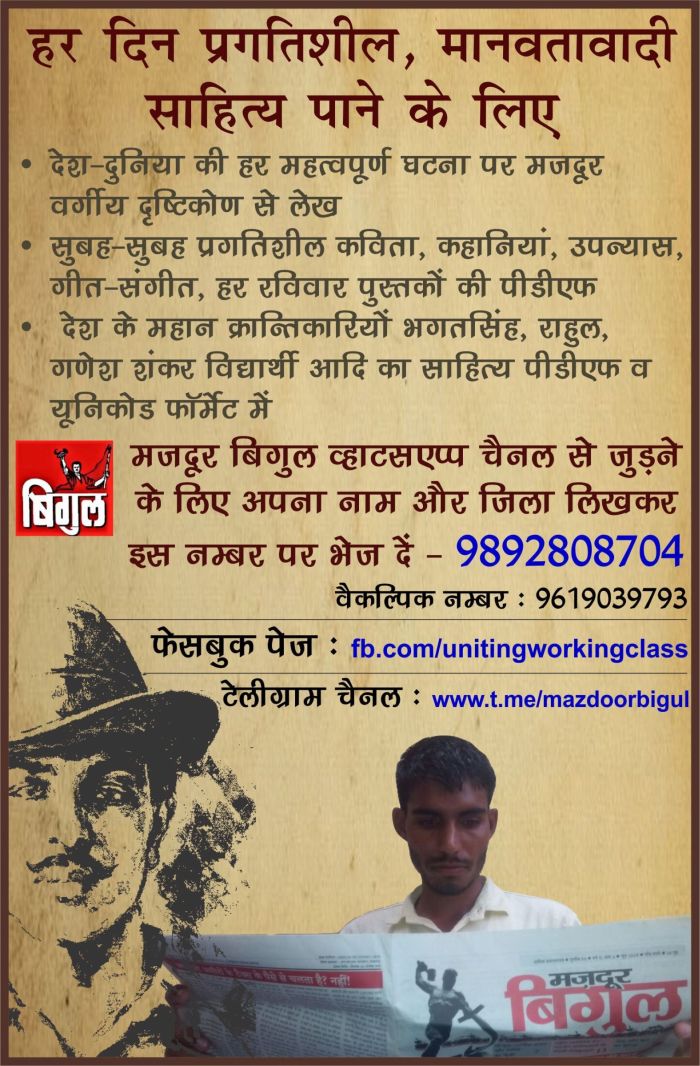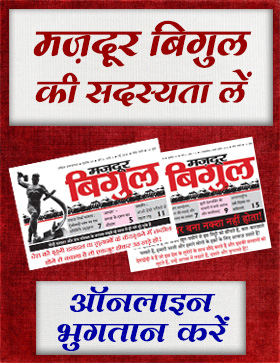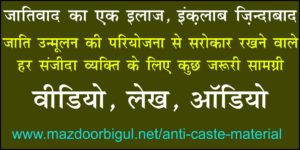‘जाति प्रश्न और मार्क्सवाद’ पर चतुर्थ अरविन्द स्मृति संगोष्ठी (12-16 मार्च, 2013), चण्डीगढ़ की रिपोर्ट
जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक मूल से लेकर उसकी गतिकी तक के बारे में अम्बेडकर की समझदारी बेहद उथली थी। नतीजतन, जाति उन्मूलन को कोई वैज्ञानिक रास्ता वह कभी नहीं सुझा सके। इसका एक कारण यह भी था कि अम्बेडकर की पूरी विचारधारा अमेरिकी व्यवहारवाद के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। लिहाज़ा, उनका आर्थिक कार्यक्रम अधिक से अधिक पब्लिक सेक्टर पूँजीवाद तक जाता था, सामाजिक कार्यक्रम अधिक से अधिक धर्मान्तरण तक और राजनीतिक कार्यक्रम कभी भी संविधानवाद के दायरे से बाहर नहीं गया। कुल मिलाकर, यह एक सुधारवादी कार्यक्रम था और पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर ही कुछ सहूलियतें और सुधार माँगने से आगे कभी नहीं जाता था।