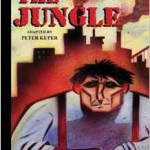इस तरह यूर्गिस को शिकागो की जरायम की दुनिया के ऊँचे तबकों की एक झलक मिली। इस शहर पर नाम के लिए जनता का शासन था, लेकिन इसके असली मालिक पूँजीपतियों का एक अल्पतन्त्र था। और सत्ता के इस हस्तान्तरण को जारी रखने के लिए अपराधियों की एक लम्बी-चौड़ी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। साल में दो बार, बसन्त और पतझड़ के समय होने वाले चुनावों में पूँजीपति लाखों डॉलर मुहैया कराते थे, जिन्हें यह फ़ौज ख़र्च करती थी – मीटिंगें आयोजित की जाती थीं और कुशल वक्ता भाड़े पर बुलाये जाते थे, बैण्ड बजते थे और आतिशबाजियाँ होती थीं, टनों पर्चे और हज़ारों लीटर शराब बाँटी जाती थी। और दसियों हज़ार वोट पैसे देकर ख़रीदे जाते थे और ज़ाहिर है अपराधियों की इस फ़ौज को साल भर टिकाये रहना पड़ता था। नेताओं और संगठनकर्ताओं का ख़र्चा पूँजीपतियों से सीधे मिलने वाले पैसे से चलता था – पार्षदों और विधायकों का रिश्वत के ज़रिये, पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव-प्रचार के फ़ण्ड से, वकीलों का तनख़्वाह से, ठेकेदारों का ठेकों से, यूनियन नेताओं का चन्दे से और अख़बार मालिकों और सम्पादकों का विज्ञापनों से। लेकिन इस फ़ौज के आम सिपाहियों को या तो शहर के तमाम विभागों में घुसाया जाता था या फिर उन्हें सीधे शहरी आबादी से ही अपना ख़र्चा-पानी निकालना पड़ता था। इन लोगों को पुलिस महकमे, दमकल और जलकल के महकमे और शहर के तमाम दूसरे महकमों में चपरासी से लेकर महकमे के हेड तक के किसी भी पद पर भर्ती किया जा सकता था। और बाक़ी बचा जो हुजूम इनमें जगह नहीं पा सकता था, उसके लिए जरायम की दुनिया मौजूद थी, जहाँ उन्हें ठगने, लूटने, धोखा देने और लोगों को अपना शिकार बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था।